तंत्र का दिव्य प्रयोग विधि
अनन्त जन्मों से एक खोज चलती रही है अपने को पहचानने की, स्वयं को जानने की,क्योंकि स्वयं को जानकर ही उस मूल स्रोत तक पहुंचा जा सकता है, उस स्रोत को ज्ञात किया जा सकता है, जहां से जीवन का अवतरण होता है। जीवन को जानकर ही जीवन से संबंधित उन मूल समस्याओं के कारणों को जाना जा सकता है, जो हमें पीड़ा, कष्ट पहुंचाते हैं। समय- असमय प्रकट होकर यह समस्यायें नाना प्रकार के दुःख-दर्द देती रहती हैं। जीवन के सत्य को जानकर ही उस शाश्वत एवं दिव्य आनन्द को प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी दिव्य अनुभूतियां कभी समाप्त नहीं होती हैं। और स्वयं को जानने का क्या अभिप्राय है ? जीवन के गूढ़तम रहस्य को जानना, इस विश्व एवं ब्रह्माण्ड को समझना, प्राकृतिक रहस्यों को आत्मसात करना, यही खोज प्राचीनकाल से आज तक चली आ रही है और यह खोज अनन्तकाल तक इसी प्रकार चलती रहेगी । मनुष्य की इस खोज के अनेक मार्ग रहे हैं। इसका एक मार्ग बाह्य विज्ञान पर आधारित रहा है, जबकि इसका दूसरा मार्ग आत्मदर्शन और स्वयं के अन्तस में गहराई से प्रवेश करने का रहा है। इन दोनों ही मार्गों की अपनी-अपनी उपयोगिताएं और अपनी-अपनी सीमाएं हैं। वैज्ञानिक मार्ग ने जीवन के अनेक रहस्यों से पर्दा अवश्य उठाया है, किन्तु इस मार्ग की सीमाएं केवल वहां तक पहुंचती हैं जहां तक प्रकृति की सीमाएं हैं। प्रकृति की सीमा से परे विज्ञान की पहुंच समाप्त हो जाती है क्योंकि वैज्ञानिकों की खोज, उनकी साधना का माध्यम वही साधन बनते हैं, जो स्वयं ही प्रकृति द्वारा निर्मित किये जाते हैं। अतः वैज्ञानिकों की खोज एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। विज्ञान के विपरीत आत्मदर्शन की खोज वहां से शुरू होती है जहां से प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है और पराभौतिक जगत की शुरूआत होती है। आत्मदर्शन की साधना में प्रकृति प्रधान वस्तु ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होती। इस साधना में पंचतत्त्व निर्मित साधक का शरीर एक आधार भर ही होता है। इस मार्ग की शुरूआत स्थूल से परे आत्मिक शरीर से होती है जिसकी चेतना का संबंध सम्पूर्ण पराभौतिक जगत एवं परमात्मा तक के साथ सदैव रहता है, लेकिन यह मार्ग वैज्ञानिक मार्ग के मुकाबले ज्यादा दुष्कर, कठिन एवं जोखिम पूर्ण है। तंत्र, योग, ध्यान आदि के रूप में जितनी भी प्रक्रियाएं प्रचलित रही हैं, वह सब आत्मदर्शन के सिद्धान्त पर ही आधारित हैं। तंत्र की प्रक्रियायें तो इन सबमें सबसे अद्भुत एवं प्रभावपूर्ण रही हैं. क्योंकि तंत्र ही एक मात्र ऐसा विज्ञान रहा है जिसकी पहुंच प्रकृति निर्मित पंच भौतिक शरीर से लेकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त आत्मिक शरीर तक, एक समान रहती है। तंत्र आध्यात्मिक जगत का एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान रहा है, जहां व्याख्या एवं विश्लेषण का ज्यादा महत्व नहीं रहा, वहां केवल प्रयोग करने एवं स्वयं तंत्र साधना की अनुभूति से गुजरने पर जोर दिया गया है। इसलिये तांत्रिक अपने शिष्यों को उपदेश अथवा प्रवचन देने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि सीधे-सीधे प्रयोगों की शुरूआत करने और स्वयं उन दिव्य क्षमताओं को प्राप्त कर लेने को कहते हैं । तंत्र प्राचीन विज्ञान की एक प्रमुख प्रयोगशाला रही है। एक समय भारत में 64 प्रकार की तंत्र विधाओं का सर्वत्र प्रचलन था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनमें से ज्यादातर तंत्र विधायें लुप्त होती चली गयी। अब तो तंत्र की 2-4 विधाओं के ही थोड़े- बहुत अंश अवशेषों के रूप में रह गये हैं। इनमें भी तंत्र के नाम पर बहुत कुछ जोड़ दिया गया है।
तंत्र विज्ञान का एक प्रमाणित ग्रंथ है- विज्ञान भैरव तंत्र । यह ग्रंथ शिव-पार्वती संवाद के रूप में संकलित हुआ है। पार्वती की जिज्ञासाओं को शांत करते हुये शिव ने तंत्र की 120 प्रक्रियाओं का रहस्योद्घाटन किया है, जिन्हें इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। तंत्र शास्त्र के इस ग्रंथ ने एक समय तंत्र विज्ञान को नई ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत मदद की थी । इस ग्रंथ में आत्मदर्शन एवं सिद्धावस्था को प्राप्त करते हुये शिव तंत्र में लीन हो जाने की 120 से ज्यादा तंत्र प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। तंत्र की यह विधियां आज भी उतनी ही प्रमाणिक एवं प्रभावपूर्ण सिद्ध होती हैं, जितनी वह सदियों पूर्व थीं । इन तंत्र विधियों के थोड़े से अभ्यास से ही कई तरह की दिव्य अनुभूतियां, कई तरह के चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। क्रियायोग, शक्ति जागरण, कुण्डलिनी जागरण, साध्य साधना, अणिमा-लघिमा जैसी अष्टसिद्धियों आदि जिन सहस्त्रों प्रक्रियाओं का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में हुआ है, उन समस्त तंत्र साधनाओं का मूल आधार यही ग्रंथ रहा है। तंत्र अनुभूति और प्रयोगों का विज्ञान रहा है किन्तु बाद में इसके साथ कई घृणास्पद एवं आडम्बरयुक्त बातें भी जुड़ती चली गयी । तांत्रिक प्रक्रियायें इतनी प्रभावपूर्ण थी कि लम्बे समय तक तंत्र गोपनीय विज्ञान ही बना रहा। एक लम्बी अवधि तक तंत्र को गुप्त बनाये रखने के प्रयास किये गये। तंत्र में घृणास्पद कुछ भी नहीं है, घृणास्पद स्वरूप तो इसे बाद में प्रदान किया गया है। इसके पीछे भी कई तरह के कारण बताये जाते हैं। तांत्रिकों के एक समूह का मानना है कि तांत्रिक क्रियाएं तत्काल असर दिखाती हैं। इन क्रियाओं की थोड़ी-बहुत क्षमताओं को अर्जित करके साधना के मार्ग से भटक जायें, तो वह समाज के लिये एक खतरो सिद्ध हो सकता है, जैसे कि आज बहुत से तांत्रिक कर रहे हैं। तंत्र साधना के मार्ग से भटके हुये थोड़ी-बहुत क्षमता सम्पन्न ऐसे तांत्रिक थोड़े लालच में ही मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन जैसे घृणास्पद कार्यों को कर डालते हैं। इन क्षमताओं के आधार पर वह लोगों को डराने, धमकाने और सताने लगते हैं। थोड़े से लोभ में यह किसी के लिये भी मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे कामों को कर देते हैं। ऐसे भटके हुये तांत्रिक लोगों को उच्चाटित करके विक्षिप्त कर डालते हैं। कृत्या (मूठ) आदि फेंक कर शारीरिक एवं मानसिक रोगी बना डालते हैं। ऐसे पतित एवं शीघ्र भटक जाने वाले लोगों का तंत्र में प्रवेश न होने पाये, इसलिये इस विधा को लम्बे समय तक गोपनीय बनाये रखा गया ।तंत्र साधना का मार्ग इतना सहज रहा है कि प्रत्येक अवस्था का व्यक्ति इस मार्ग का साधक बन सकता है। इसमें प्रवेश के लिये कोई अनिवार्य शर्त नहीं रही । तंत्र साधक बनने के लिये न तो नैतिक तैयारी की कोई जरूरत रहती है और न ही इस पर आस्था, विश्वास जमाने की आवश्यकता रहती है। यह विज्ञान है तो इसके प्रयोग करने ही पर्याप्त रहते हैं। तंत्र एक मामले में अति नैतिक कर्म रहा है जैसा कि दवायें अति नैतिक होती हैं। वह चोर या संत, सज्जन या लंपट में कोई फर्क नहीं करती, जो भी उनका प्रयोग करता है, दवा के प्रभाव से वह ठीक होता ही है। ठीक ऐसा ही तंत्र विज्ञान है। जो भी व्यक्ति तंत्र मार्ग में प्रवेश लेकर इन क्रियाओं का अभ्यास करता है, उसे तंत्र की दिव्य अनुभूतियां, तांत्रिक सिद्धियां निश्चित ही प्राप्त होती हैं। तंत्र साधना के प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते। तंत्र साधना के इस क्षेत्र से मैं स्वयं भी पिछले 25-26 वर्षों से गहराई के साथ जुड़ा रहा हूं। इस दीर्घ अवधि में अनेक बार, अनेक अवसरों पर कई तरह के अनुभवों से गुजरने का अवसर भी मिलता रहा है। इन अवसरों पर कई बार तो ऐसा लगा कि मैं स्वप्निल संसार में रह रहा हूं अथवा वास्तविक रूप से उन्हें अनुभव कर पा रहा हूं। अनेक बार वह अनुभव वास्तविक संसार के रूप में प्रतीत हुये। अपनी साधना के दौरान मैंने तंत्र विज्ञान को गहराई से समझने और स्वयं में आत्मसात करने का भी प्रयास किया। तंत्र के दिव्य प्रयोग नामक इस पुस्तक में मैं उस ज्ञान की एक झलक भर ही कहीं-कहीं दे पाया हूं, जबकि तंत्र का ज्ञान तो असीमित सागर के समान है। इस पुस्तक का मुख्य आधार साधारण लोग और उनकी भौतिक समस्यायें तथा उनका समाधान रहा है, इसलिये इस पुस्तक में तंत्र से सम्बन्धित उच्च क्रियाओं पर ज्यादा प्रकाश न डालकर, उनकी जगह उनके सूक्ष्म प्रसंग ही दे पाया हूं। यद्यपि इनके विषय में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिये जिज्ञासु पाठक मुझसे सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं हर हरसंभव तरीके से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा इस पुस्तक का मुख्य आधार जीवनकाल में समय- बेसमय पर सामने आने वाली अनेक
प्रकार की समस्याओं, बाधाओं आदि से छुटकारा पाने तक ही सीमित रहा है। जीवन की ऐसी समस्याओं एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिये तंत्र में अनेक तरह के प्रयोग, अनेक तरह की साधनाएं और अनेक तरह के उपाय खोजे जाते रहे हैं। तांत्रिकों ने अपने गहन अध्ययन के आधार पर अनेक
ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों का जगह-जगह उल्लेख किया है कि अगर उन्हें पूर्ण विधि-विधान से सम्पन्न कर लिया जाये तो निश्चित ही उन समस्याओं का निराकरण हो जाता है । मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में दिये गये तांत्रिक प्रयोग लोगों के लिये एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे। मुझे यह भी आशा है कि पुस्तक के पाठक तांत्रिक अनुष्ठानों का प्रयोग करके लाभ उठायेंगे
ही, इस प्रक्रिया में उन्हें जो अनुभूतियां प्राप्त होंगी, उनसे मुझे भी अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मैं उनके अनुभवों एवं आलोचनात्मक सुझावों का हृदय से स्वागत करूंगा। इस पुस्तक के लिये प्रेरित करने तथा समय-समय पर सुझाव देने के लिये मैं प्रकाशक श्री मोहन कुमार कश्यपजी का हृदय से आभारी हूं। उन्हीं के अमूल्य सुझावों के आधार पर ही इस पुस्तक की रूपरेखा निखर कर सामने आ पायी और मेरे अन्तस की प्रतीक्षा साक्षात रूप प्राप्त कर सकी, इसके लिये एक बार पुनः प्रकाशक महोदय साधुवाद के पात्र हैं।
समस्याओं से मुक्ति का मार्ग- तांत्रिक प्रयोग
विभिन्न प्रकार के कष्ट एवं समस्यायें मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग रही हैं । इन कष्टों तथा समस्याओं से व्यक्ति दुःखी और आहत होता है और फिर प्रयास करता है कि किस प्रकार इनसे मुक्ति प्राप्त की जाये ? अगर कहीं कष्ट और समस्यायें हैं तो निश्चित रूप से उनका समाधान भी अवश्य रहा होगा। जो सभी प्रकार के समाधान तलाश करने के उपरांत भी इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, अन्त में वे ईश्वर की शरण में आते हैं। ईश्वर को विशेष मार्ग और विधान से पुकारने पर वे अवश्य ही पुकार को सुनते हैं और पुकारने वाले साधक को कष्टों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ईश्वर तक अपनी करुण पुकार पहुंचाने के अनेक मार्ग हैं, इन्हीं में तंत्र भी एक मार्ग माना जाता है। आम लोगों के मन में तांत्रिक प्रयोगों के प्रति अच्छी राय नहीं है किन्तु तांत्रिक प्रयोगों का एक सात्विक स्वरूप भी है जो अपने इष्ट अथवा विशेष देव अथवा देवी की उपासना पर आधारित है। इष्ट अथवा किसी भी देव - देवी की पूजा तथा उपासना करने पर वे अवश्य प्रसन्न होते हैं और साधक के कष्टों को दूर करने में विलम्ब नहीं करते हैं।
इस पुस्तक में दिये गये समस्त तांत्रिक प्रयोग पूर्णतः सात्विक हैं। जो लोग इस भ्रम में है कि तंत्र साधना तांत्रिकों के काम ही आती है, उन्हें इस पुस्तक को अवश्य देखना चाहिये। पुस्तक में वर्णित उपाय अनेक साधकों द्वारा अनुभूत है। असंख्य पाठकों को इन उपायों को करने से वांछित लाभ की प्राप्ति हुई है एवं मनोकामनाओं की पूर्ति भी हुई है। तंत्र के दिव्य प्रयोग तांत्रिक अनुष्ठान, साधना, उपासना तथा प्रयोगों पर आधारित पुस्तक है। वैसे तो मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं और दुःखों से पीड़ित रहता है किन्तु इस पुस्तक में ऐसे प्रमुख अनुष्ठानों, साधनाओं तथा प्रयोगों को लिखा गया है जिनसे अधिक से अधिक पाठक लाभ ले सकें । पुस्तक में वर्णित उपाय पूरी तरह से सात्विक एवं ईश्वर के निकट ले जाने वाले हैं। लेखक आर. कृष्णा ने इस पुस्तक को सर्वकालिक उपयोगी बनाने के लिये अथक श्रम एवं शोध कार्य किया है । आर. कृष्णा ने इस पुस्तक के लेखन में अपने ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के विख्यात तांत्रिकों से सम्पर्क करके इस पुस्तक में उनके द्वारा बताये गये उपायों को सम्मिलित किया है। इस कारण से यह पुस्तक आम पाठकों के लिये अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगी। लेखक एवं प्रकाशक दोनों को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक के माध्यम से अपनी अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने में सफल रहेंगे। इस बारे में पाठकों से निवेदन है कि वे अपने विचारों से लेखक एवं प्रकाशक को अवश्य अवगत करायेंगे ।
तंत्र साधना का रहस्य
तंत्र का विषय बहुत विस्तृत और स्वयं में परिपूर्ण रहा है । इसलिये तंत्र शास्त्र को सहजरूप में, साधारण बुद्धि के साथ पूर्णरूपेण समझ पाना हर किसी के लिये संभव कभी नहीं रहा। अगर बात तंत्र साधनाओं के माध्यम से हस्तगत होने वाली क्षमताओं की, की जाये उन्हें तो समझ पाना और भी कठिन काम रहा है, क्योंकि कभी तो तांत्रिकों की बातें पूर्णतः कपोल कल्पित और साधारण ज्ञान से परे की चीजें लगती हैं और कभी तांत्रिकों के क्रियाकर्म, व्यवहार विक्षिप्तों जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तविक रूप में तो तंत्र का सम्पूर्ण विज्ञान स्थूल ज्ञान से परे आत्म अनुभूतियों पर आधारित रहा है। इसलिये तंत्र साधना की समस्त अनुभूतियां चेतन जगत से परे, साधक के अवचेतन जगत पर अवतरित होती हैं। तंत्र साधना के लिये माध्यम तो साधक का स्थूल शरीर ही बनता है, लेकिन साधना की दिव्य अनुभूतियां सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही अवतरित होती हैं। यह बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिये कि सूक्ष्म शरीर की तथा आत्मिक शरीर की अनुभतियां, स्थूल शरीर की अनुभूतियों से बहुत भिन्न रूप में रहती हैं।
हमारा स्थूल शरीर पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से अनुभूतियां संग्रहित करता है, लेकिन इन ज्ञानेन्द्रियों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। अपनी सीमा से परे के ज्ञान को यह ज्ञानेन्द्रियां पकड़ नहीं पाती हैं, किन्तु हमारे सूक्ष्म शरीर अथवा कहें कि आत्मिक शरीर की क्षमताएं स्थूल शरीर की अपेक्षा बहुत विस्तृत रूप में रहती हैं। इसलिये तंत्रादि साधनाओं के माध्यम से जो दिव्यानुभूतियां सूक्ष्म शरीर पर अवतरित होती हैं, उनके बहुत थोड़े से अंश को ही हमारा स्थूल शरीर पकड़ पाता है। यहां एक बात और भी ठीक से समझ लेने की है कि हमारे स्थूल शरीर से संबंधित जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनके ज्ञान का विकास समाज और वातावरण की देन है। इसलिये समाज हमें नाम प्रदान कर देता है । किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि से जिस नाम से परिचित करवा देता है, वही हमारा ज्ञान हो जाता है। उससे आगे की हमें कोई जानकारी नहीं होती। यही मुख्य कारण है कि किसी अपरिचित व्यक्ति के विषय में हम कुछ भी नहीं बता पाते । अगर किसी पुरुष ने अपने जीवन में पहले कभी भी किसी स्त्री को न देखा हो और न ही स्त्री से संबंधित कोई जानकारी सुनी हो, तो वह पुरुष एकाएक अपने सामने किसी स्त्री को पाकर दंग रह जायेगा, और संभव है कि वह उसे कोई भूत, प्रेत या पशु आदि समझ कर उसके सामने से भाग खड़ा हो जबकि स्वयं उसका जन्म स्त्री शरीर से ही हुआ होता है । सूक्ष्म शरीर पर अवतरित होने वाली अनुभूतियां वैसे भी चेतना जगत से परे की चीजें होती हैं। इन अनुभूतियों के विषय में समाज लगभग संज्ञाहीन ही रहता है । शायद आपने अनेक बार इस बात को तो समझा होगा कि हमारे अनुभव करने की जितनी सीमाएं हैं, उसके हजारवें अंश के बराबर भी हम अपनी अनुभूतियों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। हम अपनी अचेतना के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर पर जितना अनुभव कर पाते हैं, उसके हजारवें अंश के बराबर भी सोच-विचार नहीं कर पाते । इसी प्रकार हम जितना कुछ सोच-विचार कर पाते हैं, जितनी कल्पनाओं, जितने विचारों को अपने मन में जन्म दे पाते हैं, उनके हजारवें अंश के बराबर भी हम उन्हें शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं, अपनी अनुभूतियों को लिखने की सामर्थ्य हमारे सोचने- विचारने की क्षमता के मुकाबले हजारवें अंश के बराबर भी नहीं होती। इसलिये कोई व्यक्ति अपने अन्तस में उठने वाले विचारों को थोड़ा अधिक अंश में पकड़ कर उन्हें बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, वही समाज में सबसे अलग प्रतीत होने लग जाता है। फिर वह महान विचारक, महान लेखक, महान कवि, एक अद्भुत विद्वान के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। उसकी थोड़ी सी अधिक स्थूल क्षमता उसे सामान्य पुरुष से विशेष पुरुष अथवा महापुरुष बना देती है। लगभग यही बात तांत्रिक साधनाओं और उनके माध्यमों से उत्पन्न होने वाली क्षमताओं के विषय में भी कही जा सकती है । तांत्रिक साधनाओं और तांत्रिक अनुष्ठानों से जो क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, उनकी दिव्य अनुभूतियां चेतना से परे रहने वाले सूक्ष्म शरीर पर उतरती हैं, किन्तु उन तांत्रिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने का मुख्य आधार साधक का स्थूल शरीर और बाह्य चेतना ही बनती है । इसलिये तंत्र के माध्यम से जो दिव्य अनभूतियां साधकों को अनुभव होती हैं, वह साधारणत: स्थूल शरीर पर पूर्णत: से प्रकट ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उन्हें व्यक्त करने के लिये चेतना से संबंधित ज्ञानेन्द्रियों की सीमाएं सूक्ष्म पड़ जाती हैं। तंत्र का वास्तविक प्रकटीकरण तंत्र की दिव्य अनुभूतियों का अवतरण स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर, आत्मिक शरीर पर होता है और हममें से अधिकांश लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। इसलिये बिना तंत्र की वास्तविक अनुभूति से गुजरे हममें से अधिकतर लोग तांत्रिक साधनाओं के वास्तविक स्वरूप और उनकी क्षमताओं को समझने में पूर्णत: असमर्थ
रहते हैं। हमें एक बात और भी समझ लेनी चाहिये कि हमारे स्थूल शरीर की सीमाएं भौतिक जगत तक ही सीमित रहती हैं, जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे आत्मिक शरीर का संबंध स्थूल जगत से लेकर अभौतिक जगत तक के साथ रहता है । इस अभौतिक जगत की सूक्ष्म झांकी हममें से बहुत कम लोगों को ही कभी-कभार दिखाई पड़ती है। अधिकांश व्यक्ति तो जन्म-जन्मान्तर तक इसकी सूक्ष्म झलक से भी वंचित बने रहते हैं । अभौतिक सत्ता का यह जगत, जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं, उसकी तुलना में
सैकड़ों गुना विस्तृत है, पर हममें से अधिकतर लोग जीवन भर बाह्य चेतना के तल पर ही जीते रहते हैं, इसीलिये हमें अभौतिक जगत के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। इसी अभौतिक जगत में प्रवेश का मार्ग तंत्र साधनाएं उपलब्ध कराती हैं। हमारी बाह्य चेतना हमें स्थूल शरीर और भौतिक जगत तक ही बांधे रखती है । अतः तंत्र साधनाओं के माध्यम से साधकों के सूक्ष्म शरीर पर जिन अभौतिक शक्तियों का उदय होता है, जिन क्षमताओं का प्रकटीकरण होता है, उन्हें कुछ हद तक ही स्थूल शरीर पर अनुभव किया जा सकता है । यद्यपि शब्दों के रूप में प्रकट करना तो और भी मुश्किल होता है। अभौतिक जगत से संबंधित जिन शक्तियों का उदय सूक्ष्म शरीर पर होता है, उन्हें कुछ हद तक ही अनुभव किया जा सकता है और कुछ सीमा तक ही उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, परन्तु उन शक्तियों का सम्पूर्णता में बोध सहज एवं सामान्य बुद्धि से संभव नहीं हो पाता। उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाना तंत्र के उच्च साधकों के सामर्थ्य की ही बात होती है। एक बात और, तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से जिन शक्तियों का जागरण होता है उनका सृजनात्मक अथवा विध्वंसात्मक, किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है । इसीलिये तंत्र के वास्तविक लक्ष्य से भटके हुये कुछ तांत्रिक अपनी क्षमताओं का विनाशात्मक रूप में उपयोग करने लग जाते हैं। ऐसे तांत्रिक सृजनात्मक कार्यों की जगह मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे निकृष्ट कर्मों में अधिक रुचि लेने लगते हैं । अतः यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सही प्रक्रिया से सम्पन्न किया जाने वाला कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलता ही है । यही बात तंत्र साधना एवं तांत्रिक अनुष्ठानों पर लागू होती है । तंत्र की कोई भी साधना सम्पन्न की जाये, अगर उसकी प्रक्रिया सही है, तो उसकी कुछ न कुछ अनुभूति साधक को अवश्य होती है। साधक अपनी क्षमतानुसार उस शक्ति का उपयोग किसी विशेष रचनात्मक कार्य अथवा किसी विनाशात्मक रूप में भी कर सकता है। यद्यपि तंत्र का सम्पूर्ण रूप से उपयोग कुछ श्रेष्ठ तंत्र साधक ही कर पाते हैं । यही कारण है कि कभी-कभार ही वशिष्ठ, परशुराम, खरपानन्द, भैरवानन्द, गोरखनाथ, सर्वानन्द, मृत्युन्जय बाबा, रामकृष्ण परमहंस, वामाक्षेपा जैसा महासाधकों का जन्म होता है जो अपने तंत्र बल के आधार पर, अपनी तांत्रिक साधना के बल पर एक अलौकिक एवं विलक्षण क्षमता प्राप्त कर लेते हैं । अतः एक बात ठीक से समझ लेनी आवश्यक है कि तंत्र विज्ञान और तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से होने वाली क्षमताओं को अनुभव किया जा सकता है और उन शक्तियों का सृजनात्मक एवं विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्यों, विध्वंसात्मक अथवा। विनाशात्मक रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके उपरांत भी तंत्र की उस दिव्य शक्ति की व्याख्या करना सहज बोध से संभव नहीं हो पाता । जिस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक प्रकृति में विद्यमान रहने वाली कई तरह की शक्तियों का उपयोग करने की कला तो सीख गये हैं, वह कुछ हद तक उनके पीछे के तथ्यों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें वैज्ञानिक सिद्धान्तों के रूप 'परिभाषित करने में भी कुछ हद तक सक्षम हुये हैं लेकिन उनके लिये अब भी इस बात का उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाया है कि इन शक्तियों के अस्तित्व के पीछे प्रकृति का क्या उद्देश्य है ? इन शक्तियों का उद्देश्य क्या है ? इन शक्तियों के सृजन के पीछे किसका हाथ है ? विज्ञान सृष्टि और उसकी रचना का कुछ हद तक विश्लेषण करके संरचनात्मक बनावट की जानकारी तो दे सकता है, लेकिन हमारी इस सृष्टि का अस्तित्व क्यों है ... इसका विकास किस उद्देश्य के लिये हुआ है... जीवन की यहां क्या उपयोगिता है... मनुष्य क्या है... मनुष्य का यहां अस्तित्व क्यों है... वह कहां से आया है... किस उद्देश्य से यहां आया है... मृत्यु उपरांत वह कहां चला जाता है, इस गतिमान जगत के पीछे किसका हाथ है, ऐसे असंख्य प्रश्नों का कोई भी उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता । विज्ञान सृष्टि की बनावट अथवा मनुष्य के जीवन, उसके जीवित रहने, जन्म से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली विविध घटनाओं का विश्लेषण तो कर सकता है, परन्तु उनके पीछे के मूल उद्देश्य पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता । तंत्रशास्त्र एकमात्र ऐसा परम विज्ञान है जिसके पास सृष्टि के सभी मूल प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध है, क्योंकि तंत्र व्याख्या और विश्लेषण की जगह अनुभूति एवं साक्षात्कार पर विश्लेषण की जगह अनुभूति और साक्षात्कार पर विशेष जोर देता है। तंत्र अस्तित्व की अनुभूति पर जोर देता है। उसके लिये व्याख्यायें व्यर्थ हैं। इसलिये तंत्र की सीमाएं विराट हैं। तंत्र के लिये अस्तित्व की सीमाएं भी असीम तक विस्तीर्ण हैं। इसलिये तंत्र केवल बौद्धिक स्तर की बात नहीं करता अपितु तंत्र सदैव उस स्तर की बात करता है, जो अभौतिक जगत के साथ संबंध रखता है। यही प्रमुख कारण है कि तांत्रिक साधनाओं का बोध तो साधारण शरीर के तल पर ही संभव होने लगता है, परन्तु उसे पूर्ण रूप से आत्मसात करना साधारण शरीर से कतई संभव नहीं हो पाता । तंत्र शक्ति को स्वयं में पूर्णता के साथ आत्मसात करने के लिये आत्म रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजर कर आत्मिक स्तर, अपनी सूक्ष्म चेतना के स्तर तक पहुंचना आवश्यक होता है । सूक्ष्म जगत के स्तर पर पहुंच कर ही तंत्र और तांत्रिक शक्तियों को ठीक से समझ पाना संभव हो पाता है। यथार्थ में समस्त तंत्र साधनाओं और तांत्रिक शक्तियों का संबंध उन अभौतिक जगत की शक्तियों के साथ रहता है, जिनका विस्तार सूक्ष्म से विराट तक फैला रहता है, परन्तु उन शक्तियों का अवतरण स्थूल चेतना से परे साधक के आत्मिक चेतना के स्तर, उसके। सूक्ष्म जगत पर होता है । इन तांत्रिक शक्तियों की अनुभूति तब तक नहीं मिल पाती, जब तक कि साधना की तपस से साधक का रूपान्तरण नहीं हो जाता और उसकी अतिचेतना के सुषुप्त केन्द्र जाग्रत नहीं हो जाते । जब तक साधना के माध्यम से साधक का आत्म रूपान्तरण नहीं होता, तब तक वह छोटी-मोटी अनुभूतियां तो प्राप्त कर पाता है, लेकिन दिव्य अनुभूतियों के अनुभवों से सदैव वंचित रहता है। आत्म रूपान्तरण के बाद ही तंत्र की क्षमताओं का अवतरण हो पाता है और तभी हमें तांत्रिक सिद्धियों की झलक दिखाई पड़ने लगती है। ऐसी दिव्य अनुभूतियां साधक की बिलकुल निजी सम्पत्ति होती हैं। इनका लाभ आवश्यकता अनुसार वह दूसरों को करा तो सकता है, लेकिन यह दिव्य अनुभूतियां प्रदर्शन की वस्तु कदापि नहीं होती। इसी धरातल पर आकर साधक को अष्ट सिद्धियों का लाभ मिलने लगता । यद्यपि इनके विषय में सामान्य चेतना के साथ सोच-विचार करना कपोल कल्पनाएं ही प्रतीत होता है ।
तंत्र साधना के रूप :
तांत्रिक साधनाओं के मुख्यतः तीन रूप रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से तांत्रिकों के विभिन्न सम्प्रदाय अपने अन्तिम लक्ष्य 'परमतत्व' की प्राप्ति तक पहुंचते रहे हैं । यद्यपि इन रूपों में समयान्तराल, स्थान विशेष आदि के कारण कई प्रकार के बदलाव और नवीनताएं भी आती रही हैं। इसलिये बंगाल, कामाख्या, बिहार, गोरखपुर, नेपाल आदि के तंत्र साधकों के क्रियाकर्म और उपासना पद्धतियां हिमालय में साधानारत तांत्रिकों से काफी भिन्न प्रतीत होती हैं । तांत्रिक साधना के जो तीन रूप रहे हैं, उनमें से तंत्र साधना का प्रथम रूप आद्यशक्ति को स्वयं में पूरी तरह से आत्मसात करने की प्रक्रिया पर आधारित रहा है। साधना के इस रूप में तंत्र साधक क्षणिक भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि सम्पूर्णता के साथ परमात्मा के शाश्वत सत्य को पाना चाहता है। उसका मुख्य ध्येय शाश्वत आनन्द की अनुभूति को प्राप्त करना होता है। तंत्र साधना का यही रूप सांसारिक बंधनों से मुक्त करते हुये साधक की आत्मा को दिव्य साक्षात्कार करवा देता है। तंत्र साधना में मोक्ष, मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्ति का यही मार्ग है । इस मार्ग पर अग्रसर होते ही साधक की भौतिक आकांक्षाएं धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाती हैं और उसका प्रवेश अभौतिक संसार में होने लगता है। तंत्र साधना के इस पथ से अन्ततः साधक परमात्मा के दिव्य रूप में समाहित होता चला जाता है। तंत्र साधना का वास्तविक और श्रेष्ठ रूप यही है । तंत्र साधना के इस मार्ग पर जब कोई तांत्रिक अग्रसर होता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं तो अवश्य लोप होती चली जाती हैं, पर उसे अनंत, असीम क्षमताओं से युक्त अलौकिक शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं, जिनके माध्यम से वह प्रकृति के स्वाभाविक कार्यों में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है । यद्यपि ऐसे तंत्र साधक धीरे-धीरे इस नश्वर जगत के लिये विरक्त होने लगते हैं। उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, मान-सम्मान की भूख, सब धीरे-धीरे क्षीण और समाप्त होती चली जाती हैं । वह संसार के लिये एक अनुपयोगी प्राणी बनकर रह जाता है। इसलिये ऐसे सिद्ध तांत्रिक सांसारिक लोगों से दूर चले जाते हैं और घने जंगलों, पहाड़ों की गुप्त गुफाओं, शमशान आदि में रहने
लगते हैं । तंत्र साधना की इस उच्च अवस्था में वह सदैव समाधि की गहनावस्था और शाश्वत दिव्य आनन्द में डूबे रहना चाहते हैं। वह नश्वर जगत के वास्तविक सत्य को जान चुके होते हैं ।
यद्यपि वह अभौतिक जगत के साथ पूर्ण रूप से तारतम्य स्थापित कर चुके होते हैं, इसलिये उनकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छाएं बन जाती हैं, इसलिये प्रकृति तत्क्षण उनकी इच्छामात्र से सृष्टि के किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु को उत्पन्न कर देने के लिये तत्पर रहती है। वह इच्छामात्र से शून्य से किसी भी पदार्थ का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके लिये फिर समय की धारा कोई अवरोध खड़ा नहीं कर पाती । वह अतीत अथवा भविष्य में समान रूप से परिभ्रमण कर सकने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। उनके सामने किसी भी प्राणी का अतीत, वर्तमान अथवा भविष्य काल से संबंधित कोई भी घटना अदृश्य नहीं रह पाती। वह जीवन की समस्त घटनाओं को पकड़ सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। उनके सामने फिर पूर्वजन्मों अथवा भविष्य में होने वाले जन्मों से संबंधित घटनाएं भी किसी चलचित्र की तरह साक्षात होने लग जाती हैं। साधना की इस श्रेष्ठ अवस्था में उनकी क्षमताएं असीम रूप धारण कर लेती हैं। वह दूसरे के मन में उठने वाले विचारों को पढ़ने, पकड़ने में भी सक्षम हो जाते हैं। मनुष्यों की बात तो अलग, वह पशु-पक्षियों के साथ बात करने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिये अन्य ग्रहों का अवलोकन करना, अन्तरिक्षीय प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करना और उनसे उपयोगी कार्यों में मदद लेना भी संभव हो जाता है । इस सिद्धावस्था में पहुंचते ही साधकों की इन्द्रियां विराट का अंग बनती चली जाती हैं। वह परमात्मा की लीलाओं का अंग बनने लगती हैं। ऐसे साधकों के लिये इच्छामात्र से ही किसी भी प्राणी के भाग्य में बदलाव कर देना, किसी को भी अभयदान दे देना, किसी भी प्राणी को राजा से रंक अथवा रंक से राजा बना देना, केवल इच्छामात्र का खेल बन जाता है। यद्यपि नंश्वर संसार की वास्तविकता से गुजर चुके ऐसे संत अनावश्यक रूप में प्रकृति या परमात्मा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और प्रकृति के कार्यों, प्राणियों के जीवन को उनके सहज रूप में आगे बढ़ने देते हैं। तंत्र का यह श्रेष्ठ मार्ग है । इस सिद्धावस्था तक पहुंच पाना हर किसी के लिये सहज
रूप में संभव नहीं हो पाता । यहां तक पहुंचने के लिये तंत्र के मार्ग का अनुसरण जन्मों-जन्मों तक करना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत दुर्लभ महापुरुष ही यहां तक, इस सिद्धावस्था तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, अगस्त जैसे आद्य ऋषि, गोरखनाथ, आदिशंकराचार्य, मृत्युंजय बाबा, स्वामी महातपा, स्वामी सर्वानन्द, स्वामी
रामकृष्ण परमहंस जैसे कुछ साधक ही यहां तक पहुंचने में सफल हो पाये हैं । इस तंत्र साधना का एक रूप 'अघोर पद्धति' पर आधारित रहा है। तांत्रिकों का औघड़ सम्प्रदाय इसी तंत्र मार्ग का अनुसरण करता आ रहा है। भूतभावन भगवान भोले शंकर स्वयं इसी मत के साधक रहे हैं। औघड़ों की यह पद्धति अब भी निरन्तर जारी है। इस अघोर पद्धति पर अपनी किसी दूसरी पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखूंगा | तंत्र साधना का दूसरा रूप 'हठ योग' की पद्धति पर आधारित रहा है। इसमें तंत्र साधक हठयोग की पद्धति का अनुसरण करते हुये आत्मरूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजरते हुये अन्ततः परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है । हठयोग तंत्र, तंत्र साधना से ही संबंधित आत्मरूपान्तरण की एक विशिष्ट और वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है, जिसे तंत्र साधकों में ‘क्रियायोग' की पद्धति के नाम से जाना जाता है । इस क्रियायोग के थोड़े से अभ्यास से ही साधकों को अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव होने लग जाते हैं। वास्तव में हठयोग पद्धति पर आधारित 'क्रियायोग' अपनी अन्तः अतिचेतना में गहराई तक प्रवेश की एक अद्भुत प्रक्रिया है। यह आत्मसाक्षात्कार और समाधि जैसी सिद्धावस्था तक पहुंचने की सबसे सरल, सहज, वैज्ञानिक और अद्भुत प्रक्रिया है । इसके गहन अभ्यास से कुछ दिनों के भीतर ही साधकों को अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लग जाती हैं। इसके नियमित अभ्यास से शीघ्र ही साधकों की चेतना स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म जगत में परिभ्रमण करने लग जाती है। क्रियायोग तंत्र आधारित एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसका सर्वप्रथम प्रकटीकरण भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देते हुये अर्जुन के सामने किया था । यद्यपि बाद में आत्मसाक्षात्कार की इस जटिल प्रक्रिया को पतंजलि ने और अधिक परिष्कृत करके सरल रूप प्रदान किया । क्रियायोग संबंधी इस पद्धति पर हिमालय में तिब्बत की
सीमा में स्थित ज्ञानगंज जैसे सिद्धक्षेत्र में भी निरन्तर गहन स्वाध्याय के कार्य होते रहे हैं। इस ज्ञानगंज का संबंध आदिशंकराचार्य, गोरखनाथ, ईसा और महर्षि पुलत्स्य एवं कणाद जैसे ऋषियों से लेकर आचार्य द्रोण, माँ कृपाल भैरवी, किंकट स्वामी, स्वामी विशुद्धानन्द, योगी चैतन्यप्रज्ञ, अक्षरानन्द स्वामी, महातांत्रिक मणिसंभव आदि अनेक सिद्ध साधकों के
साथ रहा है। ज्ञानगंज नामक इस स्थान को बहुत से लोग सिद्धाश्रम या सिद्ध साधकों की स्थली आदि नामों से भी जानते हैं। यह उच्च साधना का एक ऐसा स्थल है, जहां साधना के विभिन्न रूपों पर निरन्तर अध्ययन, मनन, स्वाध्याय आदि का कार्य चलता रहता है । यह एक ऐसा सिद्ध स्थल है, जिसकी खोज अनेक पश्चिमी साधकों ने भी की है और उनमें से बहुत से लोग यहां तक पहुंचने में भी सफल रहे हैं । फ्रांस की एक लेखिका, जो बाद में
लामा बन गयी थी, एक तिब्बतीय तंत्र साधक की मदद से सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने में सफल रही थी। इसी प्रकार थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका और 'सेवन रेज' एवं 'सीक्रेट डॉक्ट्राइन' जैसी प्रसिद्ध कृतियों की लेखिका मेडम ब्लावट्रस्वी भी एक तिब्बतीय लामा की मदद से ज्ञानगंज तक पहुंचने में सफल रही थी । तिब्बतीय लामा की यह एक अशरीरी आत्मा है, जो अनेक शताब्दियों से लोगों की मार्गदर्शक बनी हुई है । आधुनिक समय में क्रियायोग नामक इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रकटीकरण काशी के महान सिद्धयोगी श्यामाचरण लाहड़ी महाशय के द्वारा किया गया था। बाद में उन्हीं की परम्परा को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। यद्यपि समय के साथ-साथ और जिज्ञासु साधकों के अभाव में सिद्ध साधकों की संख्या निरन्तर घटती चली गयी। असली क्रियावान योगी गुप्त स्थानों पर चले गये और उनकी जगह पर प्रचार-प्रसार के भूखे योगी रह गये । स्वयं लाहड़ी महाशय जी को इस क्रियायोग पद्धति की दीक्षा उनके पूर्वजन्मों के गुरु महावतार बाबा के द्वारा रानीखेत स्थित पाण्डुखोली नामक एक प्राचीन गुफा में प्रदान की थी । महावतार बाबा का संबंध भी पिछली अनेक शताब्दियों से हिमालय स्थित ज्ञानगंज आश्रम के साथ रहा है । ज्ञानगंज में महावतार बाबा को मृत्युञ्जय स्वामी की उपाधि प्रदान की गयी है, क्योंकि उन्होंने पिछली बीस-बाईस शताब्दियों से निरन्तर ज्ञानगंज और समाज के मध्य नारद की भांति संबंध स्थापित किया हुआ है। महावतार बाबा अपने कुछ सिद्ध साधकों के साथ ज्ञानगंज और हिमालय स्थित अनेक गुप्त स्थानों एवं तिब्बतीय लामाओं के गुप्त मठों में निरन्तर परिभ्रमण करते रहते हैं। बाबा जब भी किसी इच्छुक जिज्ञासु को क्रियायोग जैसी किसी पद्धति के लिये अत्यधिक लालायित अवस्था में पाते हैं, तुरन्त वायुमार्ग से उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे क्रियायोग की दीक्षा प्रदान करते हैं । यद्यपि क्रियायोग की दीक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने सांसारिक एवं विरक्त सिद्ध साधकों को सौंप रखा है। महावतार बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लाभ लेने वाले अनेक साधक अब भी साधना में रत हैं ।
ज्ञानगंज से ही संबंधित एक अन्य महापुरुष हैं, जिन्हें महर्षि महातपा के नाम से जाना जाता है। महर्षि महातपा भी अनेक शताब्दियों से क्रियायोग संबंधी अनेक प्रक्रियाओं के प्रचार-प्रसार में जुटे हुये हैं। महर्षि महातपा द्वारा भी समय-समय पर अलग-अलग साधकों को क्रियायोग की दीक्षा प्रदान करने के उल्लेख मिलते रहे हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ को उनकी तिब्बत यात्रा के दौरान इन्हीं द्वारा क्रियायोग अथवा उस जैसी ही किसी अन्य तंत्र संबंधी पद्धति की दीक्षा प्रदान की गई थी। गोरखनाथ प्रारम्भ में शाक्त उपासकों के सिद्धों के वर्ग से संबंधित रहे थे और तांत्रिकों की पंचमकार क्रियाओं का भरपूर आनन्द लूटते रहते थे । वह भी अपने गुरु मच्छन्दर नाथ की भांति मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य के भोग में निमग्न रहते थे । इन क्रियाओं का पूर्णतः भोग करने एवं इनसे विरक्त होकर ही वे कामाख्या त्यागकर हिमालय यात्रा पर निकले थे। महर्षि महातपा के द्वारा ही काशी के प्रसिद्ध संत और लाहड़ी महाशय के समकालीन प्रसिद्ध योगी त्रैलंग स्वामी को तंत्र साधना की दीक्षा प्रदान की थी । इनके अलावा मेहर बाबा, गढ़वाल के प्रसिद्ध संत गूदड़ी बाबा, नैनीताल के हेडाखान बाबा, हरिहर बाबा, बंगाल के चैतन्यपुरी और हीरानन्द स्वामी आदि अनेक ऐसे सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, जिन्हें तंत्र साधना संबंधी दीक्षाएं महर्षि महातपा के द्वारा प्रदान की गई थी । ऐसा भी माना जाता है कि महाकाली के परम साधक रामकृष्ण परमहंस जिस तंत्र साधना का नियमित अभ्यास किया करते थे और जिसके प्रभाव से उनकी परम आराध्य माँ काली स्वयं अपने हाथों से रामकृष्ण को महाप्रसाद का भोग प्रदान करने लगी थी, वह पद्धति भी क्रियायोग पर ही आधारित थी । संभवतः वह पद्धति उन्हें ज्ञानगंज से संबंधित किसी सिद्ध साधक ने प्रदान की होगी । क्रियायोग पद्धति की तरह ही हठयोग पर आधारित तंत्र साधना की एक और विशिष्ट प्रक्रिया है, जो कुण्डलिनी जागरण के निमित्त काम में लाई जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी तंत्र साधक आत्मरूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजरते हुये और कुण्डलिनी के समस्त चक्रों को क्रमशः जाग्रत करते हुये साधना के अन्तिम लक्ष्य परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है । तंत्र साधना का जो दूसरा रूप रहा है, वह उपासना एवं समर्पण की पद्धति पर आधारित है। इसमें मंत्र आदि विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं की अन्तःचेतना में जन्म-जन्मान्तर से सदैव सुषुप्तावथा में पड़ने रहने वाले चेतना केन्द्रों को जाग्रत करना होता है । इन प्रक्रियाओं के माध्यम से साधक की अन्तःचेतना अपनी इष्टदेवी के साथ जुड़ने लगती है। इनमें तंत्र साधक पूर्णतः समर्पित भाव से अपनी आराध्य शक्ति को समर्पित हो जाता है। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है, जहां साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रह जाता। दोनों का परस्पर मेल हो जाता है तथा साधक के समस्त कर्म उसके आराध्य के बन जाते हैं । तंत्र साधना की इस पद्धति के माध्यम से जैसे-जैसे साधक के चेतना केन्द्र सक्रिय और जाग्रत होते चले जाते हैं, वैसे-वैसे ही उसकी चेतना शक्ति का भी विस्तार होता चला जाता है। अन्ततः वह स्वयं विराट का अंश बनने लग जाता है। एक अवस्था के बाद अपनी साधना के माध्यम से अपनी इष्टदेवी का दिव्य साक्षात्कार पाने में भी वह सफल हो जाता है। इस साधना पद्धति की प्राचीन समय से ही दो प्रकार की प्रक्रियायें प्रचलित रही हैं। इनमें से एक प्रक्रिया विशुद्ध रूप में वैदिक पद्धति पर आधारित है, जबकि दूसरी प्रकार की प्रक्रियायें तंत्र की विविध रूपों से संबंधित रही है। तंत्र साधना का वैदिक पद्धति पर आधारित जो रूप रहा है, उसमें अभीष्ट इष्ट से सम्बन्धित मंत्रजाप, उनके स्तोत्र, रक्षा कवच, रहस्य पाठ का अभ्यास करना, विशिष्ट
प्रकार की सामग्रियों से यज्ञ, हवन करके अपने इष्ट को प्रसन्न करना मुख्य कर्म रहा है। साधना की इस प्रक्रिया में तंत्र साधक पूर्णतः समर्पित भाव से अपने इष्ट को समर्पित हो जाता है और उसके ध्यान, विभिन्न तरह के न्यास (ऋष्यादि न्यास, करन्यास, हृदयान्यास आदि) कर्मों का अभ्यास करते हुये उसे स्वयं में स्थापित कर लेता है । यह तंत्र साधना की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। दस महाविद्याओं की साधना का भी यह एक प्रमुख अंग रही है । यद्यपि इस पद्धति में पूर्ण सफलता पाने के लिये अभ्यास के साथ-साथ साधना में पूर्ण श्रद्धा, गहन आस्था, दीर्घ धैर्य और समर्पित भाव की आवश्यकता होती है । इसलिये जब तक तंत्र साधक मानसिक रूप से पूर्णतः साधना के लिये तैयार न हो जाये, तब तक उसे इस पद्धति में दीक्षित नहीं करना चाहिये अन्यथा साधना में निष्फल रहने की पूरी संभावना
बनी रहती है। हवन तंत्र साधना का जो दूसरा तांत्रिक विधान है, उसमें भी मंत्रजाप, स्तोत्र पाठ, आदि के उपक्रमों को जारी रखना पड़ता है, लेकिन इस पद्धति में साधक को मानसिक रूप से शीघ्र तैयार करने के लिये विभिन्न तरह की तांत्रिक वस्तुओं, पूजा सामग्रियों, यंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र साधना का यह एक विस्तृत विधान है और इसकी विस्तारपूर्वक यहां व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से तंत्र साधक तांत्रिक वस्तुओं और तांत्रिक क्रियाओं के रूप में ऐसी चीजों का प्रयोग भी करने लग जाते हैं, जो सामान्य साधकों के लिये घृणास्पद होती हैं। तंत्र साधना का जो तीसरा मार्ग अथवा तीसरा रूप रहा है, वह मुख्यतः क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति एवं जीवन में नित नवीन उत्पन्न होने वाली विविध तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने पर आधारित है। तंत्र साधना का यही रूप अब सर्वत्र दिखई पड़ता है। तंत्र साधना के इस रूप को ही तांत्रिक अनुष्ठान कहा जाता है। तंत्र के इस प्रचलित रूप में स्वयं साधक को आत्म रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक नहीं होता । वह जिस रूप अथवा जिस अवस्था में होता है, वहीं ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कर सकता है अथवा किसी अन्य तांत्रिक के द्वारा अपने अभीष्ट कार्य के निमित्त सम्पन्न करवा सकता है । तांत्रिक अनुष्ठानों का यह रूप है तो बहुत प्रभावशाली और इन अनुष्ठानों के चमत्कार भी शीघ्र देखने को मिलते हैं, किन्तु इनका प्रभाव सीमित समय तक ही रहता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से साधकों के विविध तरह के दुःख, दर्द, क्लेश, पीड़ाएं आदि शीघ्र समाप्त तो हो जाती हैं, पर न तो उन पर उनके इष्ट की कृपा सदैव बनी रह पाती है और न ही वह साधक दिव्य अनुभूति के स्तर तक पहुंच पाते हैं । इष्ट से साक्षात्कार, शाश्वत सत्य की उपलब्धि और आत्म साक्षात्कार जैसी कोई उपलब्धि उन्हें नहीं होती । ऐसे सभी तांत्रिक अनुष्ठान तीन पद्धतियों से सम्पन्न किये जाते हैं। इनमें एक पद्धति अघोर क्रियाओं पर आधारित है, जिसमें तांत्रिक शमशान भूमि में रहकर ऐसे समस्त अनुष्ठानों को सम्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी पद्धति वामाचार्य क्रियाओं पर आधारित रहती है, जिसमें अनुष्ठान को पूर्ण रूप से सम्पन्न करने के लिये पंचमकारों पर जोर दिया जाता है, जबकि तीसरी पद्धति शुद्ध आचरण से संबंधित वैदिक पद्धतियों पर आधारित
रहती है। तांत्रिक अनुष्ठान की इन्हीं क्रियाओं के साथ तंत्र की मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसी क्रियाओं का गहरा सम्बन्ध रहता है । इन मारण, मोहन, उच्चाटन क्रियाओं के माध्यम से एक भ्रष्ट तांत्रिक किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के समकक्ष पीड़ाएं दे सकता है।





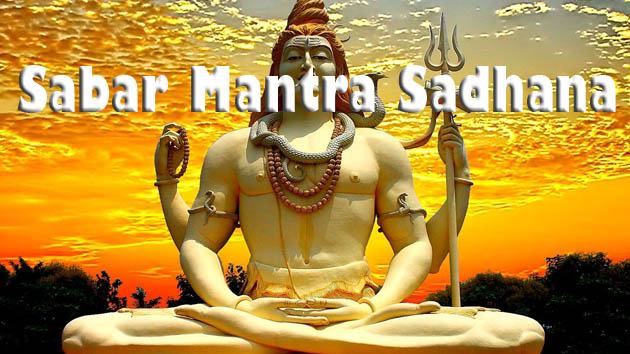




Thank you visit Mantralipi